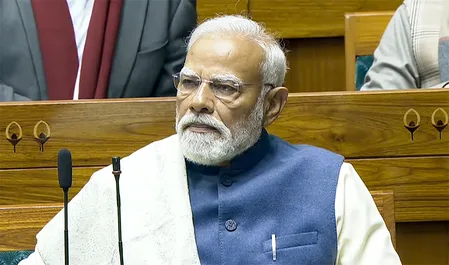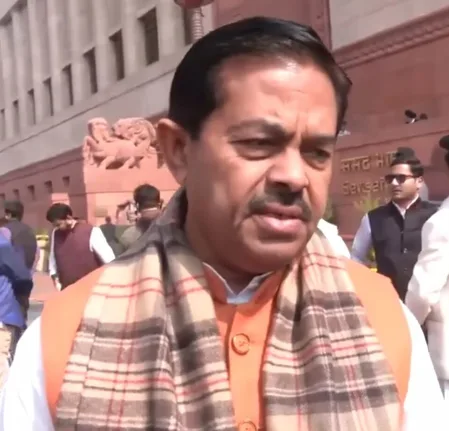सोलन में, टमाटर उत्पादक मौसम-आधारित कृषि-सलाहों को अपनाने का लाभ उठा रहे हैं, जिससे उपज में 10-12.4% की वृद्धि और खेती की लागत में 4.8-10.5% की कमी दर्ज की गई है, और अकेले कीटनाशकों के उपयोग में 2.1-14.7% की कमी आई है। यह सफलता की कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे मौसम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कृषि का संयोजन हिमाचल प्रदेश में कृषि पद्धतियों को बदल रहा है।
ये कृषि-सलाहियाँ जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन और स्मार्ट कृषि के लिए महत्वपूर्ण उपकरण साबित हो रही हैं, जिससे किसानों को बदलते मौसम के मिजाज़ के अनुकूल ढलने में मदद मिल रही है। डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के पर्यावरण विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. सतीश भारद्वाज इस बात पर ज़ोर देते हैं कि ऐसी सेवाएँ न केवल किसानों को उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर रही हैं, बल्कि उन्हें फसल बीमा लाभों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुँचने में भी सक्षम बना रही हैं। वे आगे कहते हैं कि इन सलाहों को बेहतर सटीकता और समावेशिता के साथ बढ़ाना सतत विकास लक्ष्य 2 (भूखमरी को शून्य करना) को प्राप्त करने की कुंजी है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अध्ययनों से पता चला है कि ऐसी सलाहों को समय पर अपनाने से विभिन्न फसलों, खासकर बारहमासी फलों की फसलों, जिनमें सबसे ज़्यादा लाभ होता है, में 2-5% लागत बचत और 10-25% ज़्यादा उपज होती है। हिमाचल प्रदेश में, जहाँ कृषि-जलवायु क्षेत्र विविध हैं और वर्षा आधारित बागवानी पर निर्भरता है, कृषि-सलाहें विशेष रूप से उपयोगी साबित हुई हैं।
राज्य के दोनों कृषि विश्वविद्यालय – डॉ. वाईएसपी यूएचएफ नौणी और सीएसके एचपीकेवी पालमपुर – अपनी कृषि-मौसम विज्ञान क्षेत्र इकाइयों (एएमएफयू) के माध्यम से क्षेत्र-विशिष्ट परामर्श जारी करने के लिए आईएमडी के साथ सहयोग करते हैं। राज्य में वर्तमान में चार एएमएफयू हैं, प्रत्येक विश्वविद्यालय के अंतर्गत दो। ये इकाइयाँ सेब के बागों के लिए पाले और कोहरे की चेतावनी, वर्षा-आधारित बुवाई योजनाओं और कीट/रोग प्रकोप की भविष्यवाणियों के बारे में समय पर जानकारी प्रदान करती हैं। डॉ. भारद्वाज के अनुसार, क्षेत्र-स्तरीय फीडबैक से यह पुष्टि होती है कि इन परामर्शों पर अमल करने वाले किसानों ने ओलावृष्टि, पाले और कीटों के हमलों से होने वाले फसल नुकसान को काफी कम किया है।