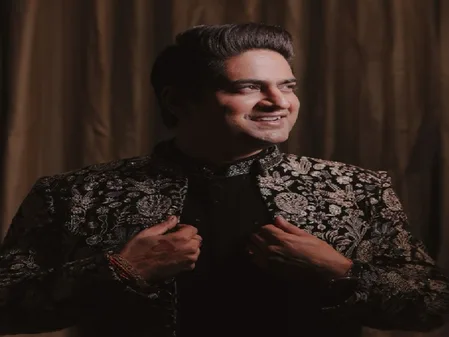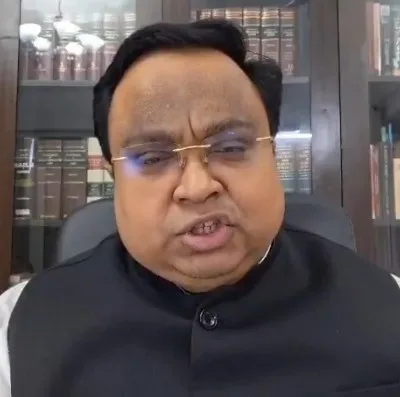जलवायु परिवर्तन का प्रभाव विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में उनके भौगोलिक, पारिस्थितिक और जलवायु परिवर्तनों के कारण देखा जाता है।
हिमालयी क्षेत्र में स्थित ये राज्य अपनी नाजुक पारिस्थितिकी प्रणालियों, अधिक ऊंचाई तथा जलवायु-संवेदनशील संसाधनों पर निर्भरता के कारण अधिकतम प्रभावों का सामना करते हैं। नीचे कुछ प्रमुख कारण दिए गए हैं कि क्यों इन राज्यों पर जलवायु परिवर्तन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है:
हिमालय दुनिया के सबसे पारिस्थितिक रूप से नाज़ुक क्षेत्रों में से एक है। इसकी खड़ी ढलानें, नई भूवैज्ञानिक संरचनाएँ और विविध सूक्ष्म जलवायु इसे जलवायु-जनित परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती हैं।
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, जहाँ गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे प्रमुख ग्लेशियर स्थित हैं, बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियरों का पिघलना तेज़ हो रहा है। जलवायु क्षेत्रों में बदलाव, पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान और पर्यटन व वानिकी पर निर्भर स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के कारण इस क्षेत्र की जैव विविधता, जिसमें दुर्लभ वनस्पतियाँ और जीव-जंतु शामिल हैं, खतरे में है।
भारी वर्षा और अचानक बाढ़: जलवायु परिवर्तन ने मानसून के पैटर्न को तीव्र कर दिया है, जिससे अनियमित और भारी वर्षा हो रही है। उत्तराखंड (जैसे, 2013 केदारनाथ बाढ़) और हिमाचल प्रदेश (जैसे, 2023 भूस्खलन और बाढ़) में विनाशकारी अचानक बाढ़ और बादल फटने की घटनाएँ हुई हैं, जो गर्म हवा में अधिक नमी के कारण और भी बढ़ गई हैं। उदाहरण के लिए, हिमाचल प्रदेश में जुलाई 2023 में अभूतपूर्व वर्षा हुई, जिससे भूस्खलन और बुनियादी ढाँचे को नुकसान पहुँचा। इसी दौरान राज्य के मंडी जिले में भी भारी तबाही देखी गई।
भूस्खलन: भारी बारिश और वनों की कटाई के कारण ढलान अस्थिर हो जाते हैं, जिससे बार-बार भूस्खलन होता है। दोनों राज्यों में भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है, अकेले हिमाचल प्रदेश में 2023 में 100 से अधिक बड़े भूस्खलन दर्ज किए जाएँगे।
सूखा काल: इन राज्यों में लम्बे समय तक सूखा काल भी रहता है, जिससे कृषि और जल विद्युत के लिए जल की उपलब्धता कम हो जाती है, जो आर्थिक आधार हैं।