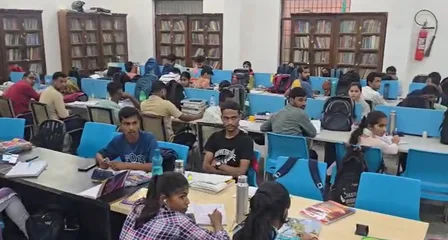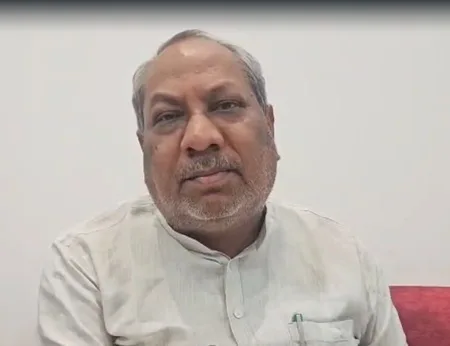ऐसे समय में जब धान के खेत हरे-भरे और लहलहा रहे होने चाहिए, पंजाब के किसान मुरझाती उम्मीदों और बौनी फसलों को देख रहे हैं। एक खामोश हमलावर – ‘बौना वायरस’ – ने एक बार फिर हमला बोला है, और इस बार लगातार तीसरे साल पंजाब के छह ज़िलों को अपनी चपेट में ले लिया है।
यह रोग, धान बौना रोग नामक विषाणु संक्रमण के कारण होता है, जो सबसे लोकप्रिय चावल की किस्म, पीआर 131, के विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है, जिससे पौधे पीले, आधे विकसित और बंजर हो रहे हैं।
इसका प्रभाव इतना विनाशकारी है कि कुछ खेतों में, पूरे के पूरे हिस्से को ट्रैक्टरों से समतल किया जा रहा है ताकि वहां पुनः पौधे रोपे जा सकें – यह कार्य निराशा और दृढ़ संकल्प दोनों का प्रतीक है।
पटियाला के गांवों में एक ही खेत में विपरीत दृश्य दिखाई देते हैं: कुछ पौधे स्वस्थ हैं, जबकि अन्य पीले, बौने और बेजान हैं।
रोपड़ के किसान गुरचरण सिंह अपनी बर्बाद फसल दिखाते हुए कहते हैं, “इसकी बढ़वार रुक गई है। अब इसे रखने का कोई मतलब नहीं है—इसमें दाने नहीं आएंगे। भारी मन से मुझे इसे जोतकर दोबारा उगाना होगा।”
यह कोई अकेली कहानी नहीं है – सैकड़ों किसानों को अब बीज, उर्वरक और ईंधन दोबारा खरीदने का बोझ उठाना पड़ रहा है, तथा इसकी कोई गारंटी नहीं है।
‘बौना वायरस’ क्या है?
वैज्ञानिकों के अनुसार, धान बौना रोग श्वेत-पीठ वाले पादप हॉपर जैसे कीटों द्वारा फैलता है, जो भोजन करते समय वायरस को संचारित करते हैं।
प्रमुख लक्षणों में शामिल हैं:
- पत्तियों का पीला पड़ना
- जड़ों की वृद्धि रुक जाना
- बौने पौधे की ऊँचाई और कम टिलरिंग
- यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो 40-50% तक फसल का नुकसान हो सकता है
सरकारी प्रतिक्रिया और वैज्ञानिक कार्रवाई
पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियाँ ने आपातकालीन प्रतिक्रिया शुरू कर दी है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) ने नुकसान का आकलन करने और मिट्टी, पानी और पौधों के नमूने एकत्र करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में विशेषज्ञ दल तैनात किए हैं।
पीएयू के वैज्ञानिकों को संदेह है कि शुरुआती मौसम में हुई बारिश और आर्द्रता ने कीटों के प्रजनन को बढ़ावा देकर वायरस के प्रसार को तेज कर दिया होगा।
किसान सलाह जारी
कृषि विभाग ने 4 सूत्री दिशानिर्देश जारी किए हैं:
- लक्षणों के लिए खेतों पर बारीकी से नजर रखें।
- घबराहट में छिड़काव करने से बचें – पहले विशेषज्ञों से परामर्श लें।
- स्थानीय कृषि विज्ञान केन्द्र या कृषि विकास अधिकारियों से तुरंत संपर्क करें।
- केवल अनुशंसित कीटनाशकों का ही प्रयोग करें – अंधाधुंध प्रयोग से स्थिति और खराब हो सकती है।